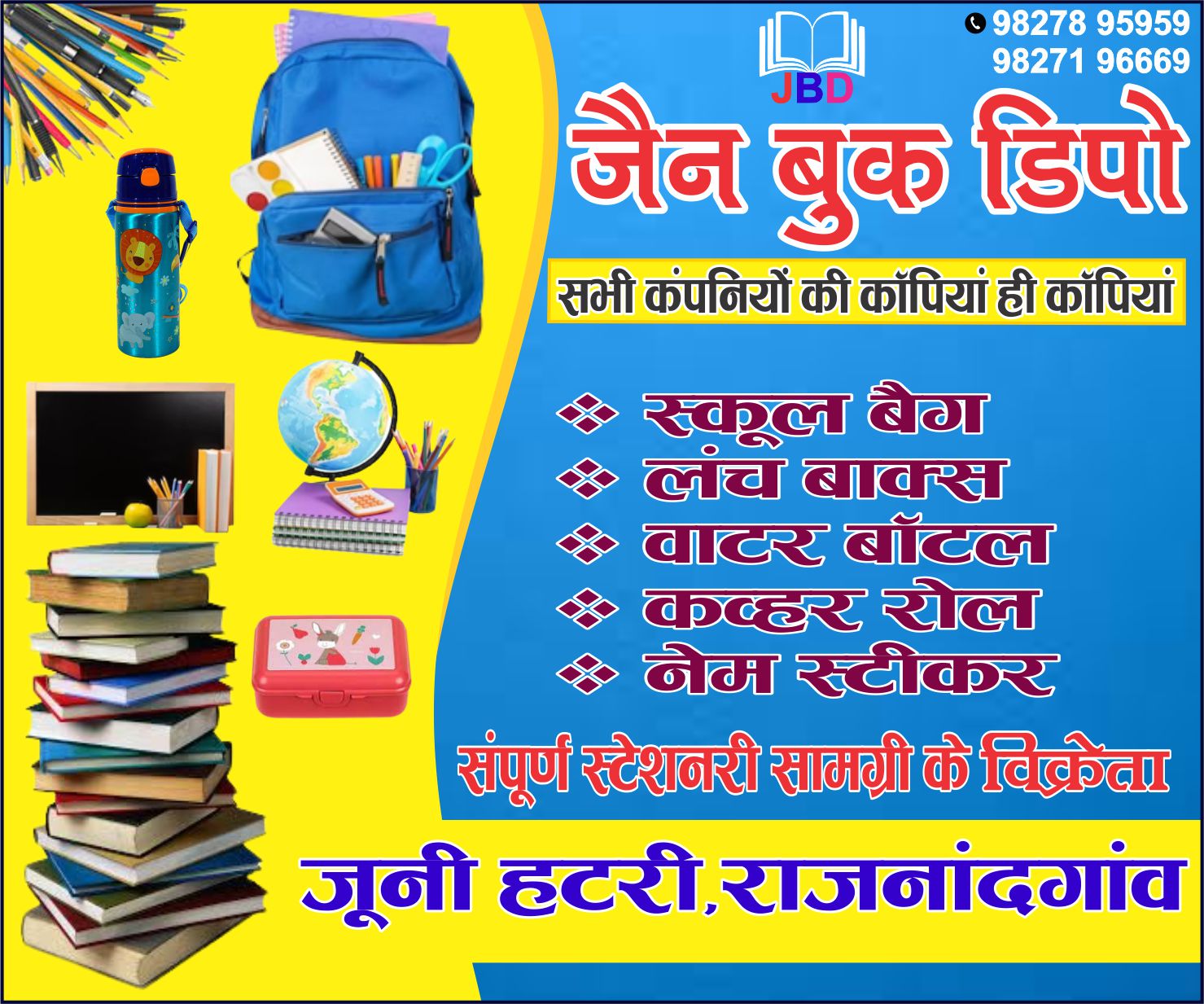Jagdeep Dhankhar On Supreme court: उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया आदेश पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि भारत में ऐसे लोकतंत्र की कल्पना नहीं की थी, जहां न्यायाधीश कानून बनाएंगे और कार्यकारी जिम्मेदारी निभाएंगे और ‘सुपर संसद’ के रूप में काम करेंगे। उपराष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का जिक्र किया, जिसमें राष्ट्रपति को तीन महीने के भीतर विधेयक पर फैसला लेने की समयसीमा तय की गई है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है, जब राष्ट्रपति को तय समय में फैसला लेने को कहा जा रहा है।
धनखड़ ने ये बातें राज्यसभा इंटर्नशिप कार्यक्रम के समापन समारोह में कही हैं। लेकिन, उन्होंने जो कुछ कहा है उसने सियासी गलियारों में ही नहीं, देश के आम लोगों में भी हलचल मचा दी है।
राज्यसभा के प्रशिक्षुओं के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि ‘एक हालिया फैसले में राष्ट्रपति को निर्देश दिया गया है। हम कहां जा रहे हैं? देश में क्या हो रहा है? हमें इसे लेकर बेहद संवेदनशील होने की जरूरत है। हमने इस दिन की कल्पना नहीं की थी, जहां राष्ट्रपति को तय समय में फैसला लेने के लिए कहा जाएगा और अगर वे फैसला नहीं लेंगे तो कानून बन जाएगा।’ उपराष्ट्रपति ने कहा कि ‘अब जज विधायी चीजों पर फैसला करेंगे। वे ही कार्यकारी जिम्मेदारी निभाएंगे और सुपर संसद के रूप में काम करेंगे। उनकी कोई जवाबदेही भी नहीं होगी क्योंकि इस देश का कानून उन पर लागू ही नहीं होता।
राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा, ‘कुछ जज कानून बनाते हैं, कार्यपालिका की भूमिका निभाते हैं और सुपर पार्लियामेंट की तरह बर्ताव करते हैं।’ उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 142 को न्यायपालिका के लिए ’24 घंटे उपलब्ध परमाणु मिसाइल’ बता दिया है। यह एक ऐसा बयान है, वह जितना तीखा है, उतना ही प्रतीकात्मक भी महसूस हो रहा है।
ज्यूडिशियल ओवररीच, ज्यूडिशियल एक्टिविज्म पर गहरी क्षुब्धता जताते हुए भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गुरुवार को विवादों का वो पैंडोरा बॉक्स खोल दिया है जिस पर भारतीय गणराज्य की लोकतांत्रिक बुनियाद टिकी हुई है। भारत का संविधान कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का बंटवारा करता है। इन तीन अंगों के बीच नियंत्रण और संतुलन (Checks and Balances) की व्यवस्था बनी है।
धनखड़ ने विधायिका और न्यायपालिका की शक्तियों और दायित्वों पर ऐसा रोषपूर्ण भाषण दिया कि सत्ता के गलियारों से लेकर न्यायपालिका की चैंबर्स तक में एक डिबेट शुरू हो गई है। धनखड़ के भाषण का मुख्य तर्क यह है कि न्यायपालिका को अपनी संवैधानिक सीमाओं का पालन करना चाहिए और लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वायत्तता का सम्मान करना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का दृष्टिकोण यह है कि वह संवैधानिकता और न्याय सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप कर सकता है।
जगदीप धनखड़ के बयान के मायने क्या?
दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल 2025 को तमिलनाडु सरकार बनाम राज्यपाल मामले में एक ऐतिहासिक फैसला दिया था। इस फैसले में कोर्ट ने कहा कि अगर राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए भेजते हैं, तो राष्ट्रपति को तीन महीने के भीतर उस पर फैसला लेना होगा। अगर विधेयक की संवैधानिकता पर सवाल हो, तो राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेनी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 201 के अनुसार, जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति को या तो उस पर सहमति देनी होती है या असहमति जतानी होती है। हालांकि, संविधान में इस प्रक्रिया के लिए कोई समयसीमा तय नहीं की गई है। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने कहा था कि कानून की यह स्थिति स्थापित है कि यदि किसी प्रावधान में कोई समयसीमा निर्दिष्ट नहीं है, तब भी वह शक्ति एक उचित समय के भीतर प्रयोग की जानी चाहिए। बेंच ने निर्देश दिया था कि हम यह निर्धारित करते हैं कि राज्यपाल द्वारा विचारार्थ भेजे गए विधेयकों पर राष्ट्रपति को उस संदर्भ की प्राप्ति की तिथि से तीन महीने के भीतर निर्णय लेना जरूरी है।
राष्ट्रपति की शक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश और वक्फ कानून जैसे मामलों में उसका हस्तक्षेप कार्यपालिका-न्यायपालिका और विधायिका-न्यायपालिका के बीच किसी किस्म के तनाव को उजागर करता है। भारत की शासन व्यवस्था में ऐसे तनाव और टकराव के मौके कम ही देखने को मिलते हैं। धनखड़ का बयान न्यायपालिका और लोकतांत्रिक संस्थाओं के बीच सीमाएं तय करने की बहस को आगे बढ़ाता है। यह केवल कानूनी मुद्दा नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र की मूलभूत संरचना से जुड़ा प्रश्न है।
क्या मर्यादा लांघ रही है न्यायपालिका?
धनखड़ की बातों से असहमति जताई जा सकती है, लेकिन उन्हें पूरी तरह से खारिज कर देना कठिन है। एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति जब सार्वजनिक मंच से न्यायपालिका की भूमिका पर सवाल उठाता है, तो वह सिर्फ व्यक्तिगत राय नहीं होती, वह लोकतांत्रिक संस्थाओं के बीच शक्ति संतुलन की जमीन पर बहस का न्योता देने जैसी होती है। भारत का संविधान स्पष्ट रूप से तीन स्तंभों – विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका – के बीच शक्तियों का विभाजन करता है और साथ ही साथ इसमें संतुलन की भी व्यवस्था कई गई है। लेकिन, हकीकत ये है कि पिछले कुछ वर्षों में न्यायपालिका की भूमिका पर यह सवाल जरूर उठने लगे हैं कि क्या वह अपने दायरे से बाहर जा रही है?